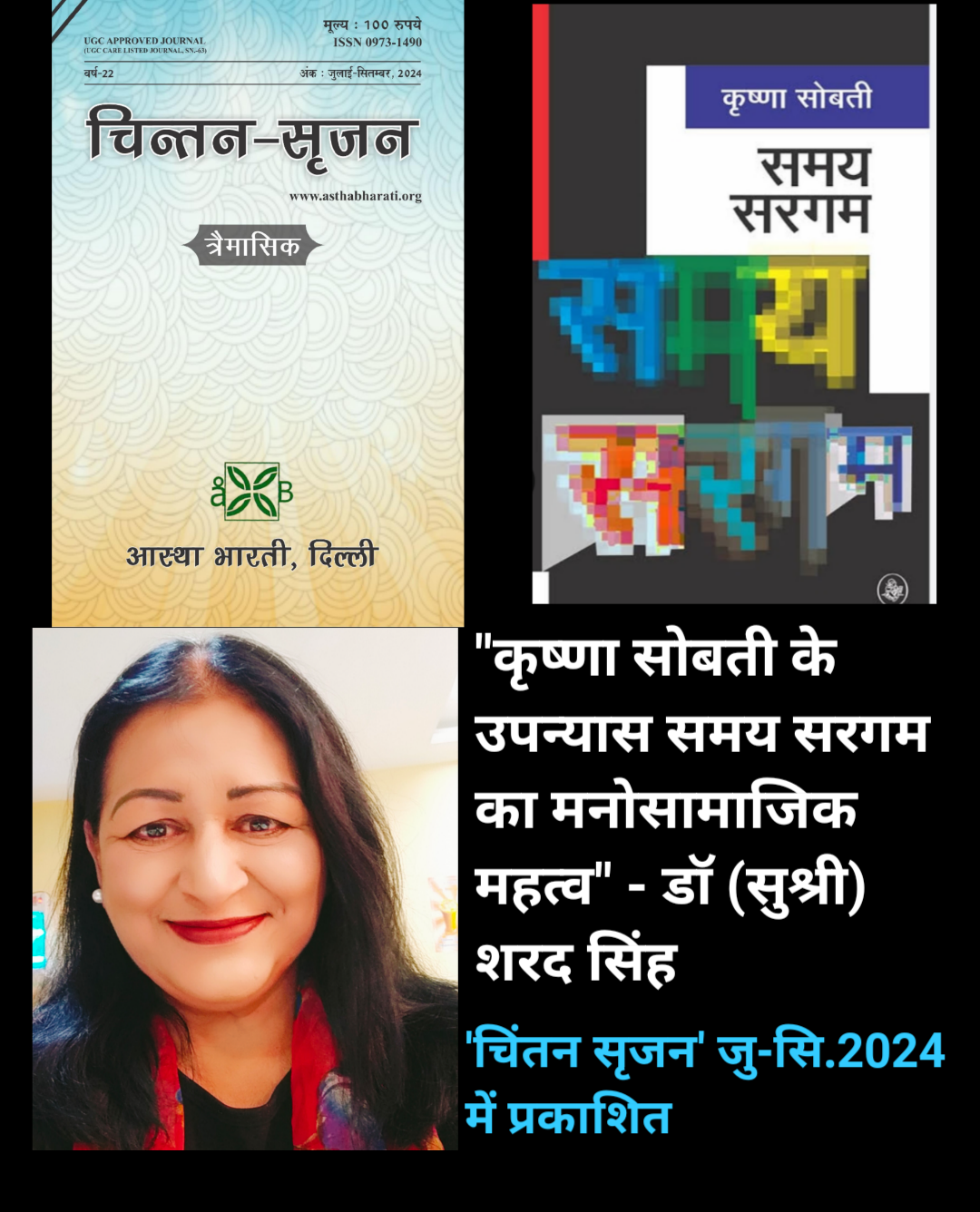आस्था भारती, दिल्ली की उच्च स्तरीय त्रैमासिक शोध पत्रिका "चिंतन-सृजन" के जुलाई सितंबर 2024 अंक में कृष्णा सोबती के उपन्यास "समय सरगम" पर केंद्रित मेरा एक शोधलेख प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है - "कृष्णा सोबती के उपन्यास 'समय सरगम' का मनोसामाजिक महत्व"।
मेरे शोध आलेख के प्रकाशन पर संपादक डॉ. शिवनारायण जी का हार्दिक आभार 🙏
--------------------------------
शोध-आलेख
कृष्णा सोबती के उपन्यास ‘समय सरगम’ का मनोसामाजिक महत्व
- डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह
कृष्णा सोबती के उपन्यास ‘समय सरगम’ का मनोसामाजिक महत्व
- डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह
प्राक्थन
समय यदि संगीत है तो आयु उसका आरोह और अवरोह है। जन्म से ले कर चरम युवा काल तक आरोह और फिर प्रौढ़ावस्था के लघु ठहराव के बाद अवरोह का स्वर फूटने लगता है। समय और आयु किसी की के लिए ठहरती नहीं है। समय का राग अपने अनेक स्वरों के साथ ध्वनित होता रहता हैै और आशाओं, अभिलाषाओं, आकांक्षाओं की स्वरलिपि आयु अनुरूप राग छेड़ती रहती है। तार सप्तक के बाद मंद सप्तक पर लौटना अनुभवों से भरे जीवन का गुरूतम स्वरूप होता है जिसे आरोही स्वर अवरोह का थका हुआ स्वर मान लेते हैं और अपनी स्फूर्ति पर इठलाते हुए मंद-सप्तक स्वरों को बोझ समझने लगते हैं। यही समय और आयु का सत्य है और मानव के सामाजिक जीवन का भी। कृष्णा सोबती के उपन्यास ‘‘समय सरगम’’ में जीवन के स्वरों के अवरोह का भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्पष्टता से उसी बेबाकी से किया गया है, जिसके लिए उनका लेखनकर्म ख्यातिलब्ध रहा है। समाज द्वारा गढ़े गए उस मनोविज्ञान का भी विश्लेषण इस उपन्यास में है जो वृद्धजन की सामाजिक एवं मानसिक स्थितियों से साक्षात्कार कराता है।
कृष्णा सोबती का जीवन
कृष्णा सोबती हिन्दी की लेखिकाओं में वह क्रांतिकारी नाम है जिसने खुल कर, साहस के साथ कलम चलाई और वे कभी डरी या घबराई नहीं। वे अपने लेखन के साथ समाज के कट्टरपंथियों के सामने डट कर खड़ी रहीं। कृष्णा सोबती का जन्म पंजाब प्रांत के गुजरात नामक उस हिस्से में 18 फरवरी 1925 को हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने आरम्भ में लाहौर के फतेहचंद कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत की थी, परंतु जब भारत का विभाजन हुआ तो उनका परिवार भारत लौट आया। कृष्णा सोबती की शिक्षा दिल्ली और शिमला में हुई।
कृष्णा सोबती को अपने कथापात्रों के मनोविज्ञान को अपने उपन्यासों और कहानियों में उतारने में महारत हासिल थी। उनके सभी पात्र प्रखर होते थे। विशेषरूप से उनकी कहानियों के स्त्री पात्र अपने अस्तित्व के लिए आवाज बुलंद करने वाले होते थे, जिसके कारण वे कई बार विवादों में भी रहीं। उन्होंने जिंदगीनामा, डार से बिछुड़ी, मित्रो मरजानी, यारों के यार, तिन पहाड़, समय सरगम, जैनी मेहरबान सिंह, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान, ऐ लड़की, दिल-ओ-दानिश और चन्ना जैसे उपन्यास लिखें।
लेखन में निर्भीकता, खुलापन और भाषागत प्रयोगशीलता ये तीन विशेषताएं कृष्णा सोबती को अपने समकालीन लेखिकाओं से अलग करती हैं। सामाजिक बंदिशों के समय में अपने स्त्री समाज के प्रति मुखर होना उनके आंतरिक साहस को रेखांकित करता है। सन् 1950 में कहानी ‘‘लामा’’ से अपनी साहित्यिक यात्रा आरंभ करने वाली कृष्ण सोबती स्त्री की स्वतंत्रता और न्याय की पक्षधर थीं। उन्होंने समय और समाज को केंद्र में रखकर अपनी रचनाओं में एक युग को गढ़ा। अपने लेखन के बारे में उनका कहना है कि ‘‘मैं बहुत नहीं लिख पाती हूं। मैं तब तक कलम नहीं चला पाती हूं, जब तक अंदर की कुलबुलाहट और उसे अभिव्यक्त करने का दबाव इतना अधिक न बढ़ जाए कि मैं लिखे बिना न रह सकूं।’’
उन पर यह आक्षेप लगाया जाता रहा है कि एक स्त्री होने के बाबजूद ‘‘यारों के यार’’ और ‘‘मित्रों मरजानी’’ में उन्होंने उन्मुक्त भाषा (बोल्ड) का प्रयोग किया जबकि वे भली-भांति जानती थीं कि उन पर ‘‘अश्लील लेखन’’ के आरोप लगेंगे। अपने एक विदेशी रेडियो साक्षात्कार में उन्होंने ‘‘अश्लील लेखन’’ के आरोप पर खुल कर अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था कि - ‘‘भाषिक रचनात्मकता को हम मात्र बोल्ड के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लेखक और भाषा दोनों के साथ अन्याय करेंगे। भाषा लेखक के बाहर और अंदर को एकसम करती है। उसकी अंतरदृष्टि और समाज के शोर को एक लय में गूंथती है। उसका ताना-बाना मात्र शब्द कोशी भाषा के बल पर ही नहीं होता। जब लेखक अपने कथ्य के अनुरूप उसे रुपांतरित करता है तो कुछ ‘नया’ घटित होता है। मेरी हर कृति के साथ भाषा बदलती है। मैं नहीं, वह पात्र है जो रचना में अपना दबाव बनाए रहते हैं। ‘जिन्दगीनामा’ की भाषा खेतिहर समाज से उभरी है। ‘दिलोदानिश’ की भाषा राजधानी के पुराने शहर से है, नई दिल्ली से नहीं। उसमें उर्दू का शहरातीपन है। ‘ऐ लड़की’ में भाषा का मुखड़ा कुछ और ही है। उसकी गहराई की ओर संकेत कर रही हूं।’’
कृष्णा सोबती को सन 1980 में जिंदगीनामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1981 में शिरोमणि पुरस्कार के अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1982 में कृष्णा सोबती को हिंदी अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सन 1996 में कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी फेलोशिप से पुरस्कृत किया गया। सन 1999 में, लाइफटाइम लिटरेरी अचीवमेंट अवार्ड के साथ कृष्णा सोबती प्रथम महिला बनीं जिन्हें कथा चूड़ामणि अवार्ड से नवाजा गया। सन 2008 में हिंदी अकादमी दिल्ली का ‘शलाका अवार्ड’ भी उनको मिला तथा सन 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
एक दिलचस्प बात जिसके बारे में उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में बताया था कि उपन्यास ‘जिंदगीनामा’ सन् 1952 में लिख कर प्रकाशक के पास भेजा किन्तु प्रकाशक ने उसकी भाषा पर आपत्ति करते हुए उसमें परिवर्तन करने को कहा। कृष्णा सोबती को यह स्वीकार्य नहीं हुआ और उन्होंने उसे प्रकाशक से वापस ले लिया। अंततः वह उपन्यास सन् 1979 में प्रकाशित हुआ और उस पर उन्हें 1980 साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। यद्यपि कुछ दशक बाद उन्होंने असहिष्णुता के मुद्दे पर साहित्य अकादमी अवार्ड सहित हिंदी अकादमी का ‘शलाका सम्मान’ और ‘व्यास सम्मान’ भी लौटा दिया था। इतना ही नहीं उन्होंने ‘पद्मभूषण’ लेने से भी मना कर दिया था। ऐसी दृढ़ और जीवट लेखिका के बारे जानने की जिज्ञासा हर साहित्यकार के मन में होना स्वाभाविक है।समय यदि संगीत है तो आयु उसका आरोह और अवरोह है। जन्म से ले कर चरम युवा काल तक आरोह और फिर प्रौढ़ावस्था के लघु ठहराव के बाद अवरोह का स्वर फूटने लगता है। समय और आयु किसी की के लिए ठहरती नहीं है। समय का राग अपने अनेक स्वरों के साथ ध्वनित होता रहता हैै और आशाओं, अभिलाषाओं, आकांक्षाओं की स्वरलिपि आयु अनुरूप राग छेड़ती रहती है। तार सप्तक के बाद मंद सप्तक पर लौटना अनुभवों से भरे जीवन का गुरूतम स्वरूप होता है जिसे आरोही स्वर अवरोह का थका हुआ स्वर मान लेते हैं और अपनी स्फूर्ति पर इठलाते हुए मंद-सप्तक स्वरों को बोझ समझने लगते हैं। यही समय और आयु का सत्य है और मानव के सामाजिक जीवन का भी। कृष्णा सोबती के उपन्यास ‘‘समय सरगम’’ में जीवन के स्वरों के अवरोह का भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्पष्टता से उसी बेबाकी से किया गया है, जिसके लिए उनका लेखनकर्म ख्यातिलब्ध रहा है। समाज द्वारा गढ़े गए उस मनोविज्ञान का भी विश्लेषण इस उपन्यास में है जो वृद्धजन की सामाजिक एवं मानसिक स्थितियों से साक्षात्कार कराता है।
कृष्णा सोबती का जीवन
कृष्णा सोबती हिन्दी की लेखिकाओं में वह क्रांतिकारी नाम है जिसने खुल कर, साहस के साथ कलम चलाई और वे कभी डरी या घबराई नहीं। वे अपने लेखन के साथ समाज के कट्टरपंथियों के सामने डट कर खड़ी रहीं। कृष्णा सोबती का जन्म पंजाब प्रांत के गुजरात नामक उस हिस्से में 18 फरवरी 1925 को हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने आरम्भ में लाहौर के फतेहचंद कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत की थी, परंतु जब भारत का विभाजन हुआ तो उनका परिवार भारत लौट आया। कृष्णा सोबती की शिक्षा दिल्ली और शिमला में हुई।
कृष्णा सोबती को अपने कथापात्रों के मनोविज्ञान को अपने उपन्यासों और कहानियों में उतारने में महारत हासिल थी। उनके सभी पात्र प्रखर होते थे। विशेषरूप से उनकी कहानियों के स्त्री पात्र अपने अस्तित्व के लिए आवाज बुलंद करने वाले होते थे, जिसके कारण वे कई बार विवादों में भी रहीं। उन्होंने जिंदगीनामा, डार से बिछुड़ी, मित्रो मरजानी, यारों के यार, तिन पहाड़, समय सरगम, जैनी मेहरबान सिंह, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान, ऐ लड़की, दिल-ओ-दानिश और चन्ना जैसे उपन्यास लिखें।
लेखन में निर्भीकता, खुलापन और भाषागत प्रयोगशीलता ये तीन विशेषताएं कृष्णा सोबती को अपने समकालीन लेखिकाओं से अलग करती हैं। सामाजिक बंदिशों के समय में अपने स्त्री समाज के प्रति मुखर होना उनके आंतरिक साहस को रेखांकित करता है। सन् 1950 में कहानी ‘‘लामा’’ से अपनी साहित्यिक यात्रा आरंभ करने वाली कृष्ण सोबती स्त्री की स्वतंत्रता और न्याय की पक्षधर थीं। उन्होंने समय और समाज को केंद्र में रखकर अपनी रचनाओं में एक युग को गढ़ा। अपने लेखन के बारे में उनका कहना है कि ‘‘मैं बहुत नहीं लिख पाती हूं। मैं तब तक कलम नहीं चला पाती हूं, जब तक अंदर की कुलबुलाहट और उसे अभिव्यक्त करने का दबाव इतना अधिक न बढ़ जाए कि मैं लिखे बिना न रह सकूं।’’
उन पर यह आक्षेप लगाया जाता रहा है कि एक स्त्री होने के बाबजूद ‘‘यारों के यार’’ और ‘‘मित्रों मरजानी’’ में उन्होंने उन्मुक्त भाषा (बोल्ड) का प्रयोग किया जबकि वे भली-भांति जानती थीं कि उन पर ‘‘अश्लील लेखन’’ के आरोप लगेंगे। अपने एक विदेशी रेडियो साक्षात्कार में उन्होंने ‘‘अश्लील लेखन’’ के आरोप पर खुल कर अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था कि - ‘‘भाषिक रचनात्मकता को हम मात्र बोल्ड के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लेखक और भाषा दोनों के साथ अन्याय करेंगे। भाषा लेखक के बाहर और अंदर को एकसम करती है। उसकी अंतरदृष्टि और समाज के शोर को एक लय में गूंथती है। उसका ताना-बाना मात्र शब्द कोशी भाषा के बल पर ही नहीं होता। जब लेखक अपने कथ्य के अनुरूप उसे रुपांतरित करता है तो कुछ ‘नया’ घटित होता है। मेरी हर कृति के साथ भाषा बदलती है। मैं नहीं, वह पात्र है जो रचना में अपना दबाव बनाए रहते हैं। ‘जिन्दगीनामा’ की भाषा खेतिहर समाज से उभरी है। ‘दिलोदानिश’ की भाषा राजधानी के पुराने शहर से है, नई दिल्ली से नहीं। उसमें उर्दू का शहरातीपन है। ‘ऐ लड़की’ में भाषा का मुखड़ा कुछ और ही है। उसकी गहराई की ओर संकेत कर रही हूं।’’
कृष्णा सोबती को सन 1980 में जिंदगीनामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1981 में शिरोमणि पुरस्कार के अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1982 में कृष्णा सोबती को हिंदी अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सन 1996 में कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी फेलोशिप से पुरस्कृत किया गया। सन 1999 में, लाइफटाइम लिटरेरी अचीवमेंट अवार्ड के साथ कृष्णा सोबती प्रथम महिला बनीं जिन्हें कथा चूड़ामणि अवार्ड से नवाजा गया। सन 2008 में हिंदी अकादमी दिल्ली का ‘शलाका अवार्ड’ भी उनको मिला तथा सन 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
25 जनवरी 2019 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।
‘समय सरगम’ का मनोसामाजिक विश्लेषण एवं महत्व
वृद्धावस्था जीवन की एक अनिवार्य स्थिति है। व्यक्ति जब तक युवा रहता है तब तक उसमें स्फूर्ति का सागर हहराता रहता है। किन्तु वृद्धावस्था दैहिक ऊर्जा को निरंतर क्षीण करती जाती है। उस समय उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है पारिवारिक एवं सामाजिक मनोबल की, अपनत्व की और सहारे की। ऐसी अवस्था में यदि किसी व्यक्ति को एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो वह छोटे-छोटे सहारे को भी बड़ा मान बैठता है। वस्तुतः यह एक जटिल मानसिक स्थिति है।
‘समय सरगम’ कृष्णा सोबती का एक अनूठा उपन्यास है। यह समय की गति को उसकी नब्ज़ और सामाजिक दुरावस्थाओं के साथ जांचता है। ‘समय सरगम’ को पढ़ते हुए सहसा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का संस्मरणात्मक निबंध ‘वृद्धावस्था’ याद आता है जिसमें उन्होंने लिखा है -‘‘काल की बड़ी क्षिप्र गति है। वह इतनी शीघ्रता से चला जाता है कि सहसा उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हम लोग मोहावस्था में पड़े ही रहते हैं और एक-एक पल, एक-एक दिन और एक-एक वर्ष कर काल हमारे जीवन को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चुपचाप ले जाता है। जब कभी किसी एक विशेष घटना से हमें अपनी यथार्थ अवस्था का ज्ञान होता है तब हम अपने में विलक्षण परिवर्तन देखकर विस्मित हो जाते हैं। उस समय हमें चिंता होती है कि अब वृद्धावस्था आ गई है, अब हमें अपने जीवन का हिसाब पूरा कर देना चाहिए। दर्पण में प्रतिदिन ही हम अपना मुख देखते हैं, पर अवस्था का प्रभाव इतने अज्ञात रूप से होता है कि हम अपने मुख पर कोई परिवर्तन नहीं देख पाते। कान के पास बालों को सफेद देखकर राजा दशरथ को एक दिन सहसा ज्ञात हुआ कि अब उनकी वृद्धावस्था आ गई। उस दिन निर्मला से परिचित होने पर मुझे भी सहसा ज्ञात हुआ कि मैं अब वृद्ध हो गया हूं।’’
अवस्था चाहे कोई भी हो प्रायः किसी अन्य व्यक्ति के बोध कराने पर अनुभव होती है, वृ़़द्धावस्था तो विशेषरूप से। बच्चे आयु में कितने भी बड़े हो जाएं किन्तु माता-पिता की दृष्टि में बच्चे ही रहते हैं। पचास वर्षीय संतान को भी चोट लगती है तो मां को ठीक उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि उसे शैशवावस्था में चोट लगने पर पीड़ा होती थी। इसके विपरीत मां की गोद में छिप कर सारे संसार के भय, निराशा और क्रोध से मुक्ति पा लेने वाली संतान जब आत्मनिर्भर हो जाती है तब उसे अपनी वही मां अनापेक्षित लगने लगती है। वह अपनी अशक्त हो चली मां को वह संरक्षण, वह सहारा, वह स्नेह देने को तैयार नहीं होता है जो उसने अपनी मंा से पाया था।
वृद्धावस्था का अहसास उस पल पहली बार होता है जब अपनी ही संतान द्वारा अवहेलना का शिकार होना पड़ता है वहीं वृद्धावस्था समाज द्वारा ‘बेचारी’ अवस्था के रूप में देखे जाने के कारण भी व्यक्ति को तोड़ने लगती है। ‘समय सरगम’ में दो प्रमुख पात्र हैं- आरण्या और ईशान। दोनों वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। वह अवस्था जिसे ‘सीनियर सिटिजन’ के सम्बोधन से खोखला सम्मान तो दे दिया जाता है किन्तु सत्यता इससे परे कटु से कटुतर होती है। ईशान बाल-बच्चेदार व्यक्ति हैं किन्तु उनके बेटे उन्हें अपने साथ नहीं रखते हैं। ईशान अकेले रहते हैं और इस बात की प्रतीक्षा रहती है उन्हें कि उन्हीं पोती अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्हें फोन करेगी और बुलाएगी। यह अल्प सुख ईशान के भीतर जीवित रहने की जिजिविषा बनाए रखता है। यह सच है कि आरण्या के साथ ने उनके जीवन में उत्साह का संचार किया। वहीं आरण्या एकाकी महिला है। जीवन जीने की दिशा में ईशान से कहीं अधिक स्फूत्र्त। वह लेखिका है। शायद इसी लिए उसका एकाकीपन उसे नैराश्य से बचाए रखता है। दोनों व्यक्ति दिल्ली महानगर में रहते हैं। दोनों दिल्ली विकास प्राधिकरण के आभारी हैं जिसने ऐसे पार्क बना रखे हैं जहां जवान, बूढ़े हर कोई घूम सकता है, हल्के-फुल्के व्यायाम करते हुए परस्पर एक दूसरे से परिचित हो सकता है। वृद्धों के लिए ऐसी जगह सबसे आरामदेह है। ‘‘बूढ़ों सयानों की टोली हर शाम इस छोटे से बगीचे में पहले टहलती है, फिर बतियाती है। डी.डी.ए. की बदौलत। नागरिक कृतज्ञ हैं इस छुटके से बगीचे में बिछी हरियाली घास के लिए। फूलों की क्यारियों और लतरों के लिए। न होता ये सुहाना टुकड़ा तो देखती रहती यह अंाखें सीमेंट के अपार्टमेंट जंगल को।’’ (पृ.89)
खुली हवा में सांस लेते हुए अपने हमउम्रों के दुख-सुख को बांटने का एक अलग ही आनन्द है। लेकिन पार्क से लौटते ही वही एकाकीपन। इस एकाकीपन के पास कृष्णा सोबती कैसे पहुंची? कैसे उन्हें उस पीड़ा का अहसास हुआ कि अकेले वृद्ध किस तरह खुशियों के एक-एक कतरे के लिए तरसते हैं? इस तारतम्य में उनका स्वयं का कथन बहुत अर्थ रखता है-‘‘मैं उस सदी की पैदावार हूं जिसने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ छीन लिया। यानी एक थी आजादी और एक था विभाजन। मेरा मानना है कि लेखक सिर्फ़ अपनी लड़ाई नहीं लड़ता और न ही सिर्फ़ अपने दुख-दर्द और खुशी का लेखा-जोखा पेश करता है। लेखक को उठना होता है, भिड़ना होता है। हर मौसम और हर दौर से नज़दीक और दूर होते रिश्तों के साथ, रिश्तों के गुणा और भाग के साथ, इतिहास के फैसलों और फ़ासलों के साथ। मेरे आसपास की आबोहवा ने मेरे रचना संसार और उसकी भाषा को तय किया। जो मैंने देखा, जो मैंने जिया वही मैंने लिखा ‘ज़िन्दगीनामा’, ‘दिलोदानिश’, ‘मित्रो मरजानी’, ‘समय सरगम’, ‘यारों का यार’ में।’’ (बीबीसी हिन्दी डाॅट काॅम, 18 अगस्त 2004)
कथानक भले ही एकाकी वृद्धों के जीवन पर केन्द्रित हो किन्तु देश के बंटवारे का दर्द ‘समय सरगम’ में भी अपनी सम्पूर्णता के साथ दिखाई पड़ता है। ‘‘नई पुरानी दिल्ली अपनी घनी सजीली छब में हर हाल में अपनी सूरत और सीरत सम्हाले रहती। आज़ादी के साथ ही राजधानी में बाढ़ की तरह रेला उठ आया। आक्रामक विस्थापितों के ठट्ठ के ठट्ठ। यहां-वहां सब जगह। शहर के हर इलाके में। दिल्ली निवासी शरणार्थियों की भीड़ से परेशान और गंाव-कस्बों और शहरों से उखड़े हुए आक्रामक शरणार्थी-दिल्ली के सुसंस्कृत मिज़ाज में घूल भरी आंधियां चलने लगीं।’’ (पृ.43)
शरणार्थी अपने और अपनों के जीवन के लिए आक्रामक मुद्रा में भले ही थे किन्तु अधिकांश ऐसे थे जो अकेले रह गए थे। अतः अकेलेपन की चर्चा के समय देश के बंटवारे के दौरान उपजा अकेलापन भी विषयानुकूल है। पहले भरपूरा परिवार पारम्परिक और संस्कृति से ओतप्रोत फिर एक लम्बा अकेला जीवन। यह बंटवारे के समय परिस्थिति का परिणाम रहा किन्तु वर्तमान में यह प्रारब्ध बन गया है। दिल्ली जैसे महानगरों की गंगनचुम्बी इमारतों के छोटे-छोटे फ्लैट्स में एकल परिवार और अकेले बूढ़ों की वो दुनिया बस गई है जिनके बीच स्नेह की बेल सूख चुकी है। आरण्या और ईशान संयुक्त परिवार की अवधारणा के समाप्त होने पर चर्चा करते हैं तो आरण्या बोल उठती है-‘‘ईशान, मुझे संयुक्त परिवार का अनुभव नहीं। दूर-पास से जो इसकी आवाज़ें सुनीं वह सुखकर नहीं थीं। इतना जानती हूं कि परिवार की सुव्यवस्थित अस्मिता ओर गरिमा का मूल्य भी उनहें ही चुकाना होता है जिनका खाता दुबला हो। परिवार की सांझी श्री पैसे के व्यापारिक प्रबंधन में निहित है। उसकी आंतरिक शक्ति क्षीण हो चुकी है। घनी छांह की जगह घिसी हुई पुरानी चिन्दियां फरफरा रही हैं। जानती हूं ईशान, आपको यह बात ठीक नहीं लग रही, पर मैं अपनी कीमत पर इसकी पड़ताल कर रही हूं और ‘सत्य’ के नाना-रूप में संचारित छोटे-बड़े झूठ और झूठों से बनाए गए स्वर्णिम सत्यों की ठोंक-पीट ही इस सात्विक संसार की प्रेरणा है।’’ (पृ.64)
यदि वृद्धावस्था आ गई है तो क्या चैबीस घंटे ईश्वर की स्तुति एवं धर्म-दर्शन में व्यतीत करना चाहिए? ईशान आरण्या का परिचय दमयंती से कराता है। वह भी उनकी हमउम्र है। किन्तु वह इन दोनों की भांति एकाकी नहीं है वरन् अपने बेटों-बहुओं के साथ रह रही है। उसने समाज एवं परिवार की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप स्वयं को एक गुरु की शिष्या बना कर सत्संग के हवाले कर दिया है। ऊपर से देखने से यही लगता है कि वह अपनी इस स्थिति से प्रसन्न एवं संतुष्ट है। वास्तविकता इससे परे है। दमयंती का खान-पान गुरू के निर्देशानुसार बदल चुका है। पहनावा भी उन्हीं के अनुसार अपना लिया है। लेकिन बेटे, बहू फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। दमयंती मानो किसी भुलावे में जी रही है। वह कहती है-‘‘आरण्या, मैं सूती कपड़ा तन को छुआती न थी। एक दिन सत्संग के बाद मेरी गुरूजी ने टोक दिया। अब सूफियाने-से सूती जोड़े बनवाए हैं। मेरे बेटों और बहुओं की सुनो। रेशम पहनो तो कहते हैं, इस उम्र में ये मचक-दमक अच्छी नहीं लगती। सूती पहनूं तो वह भी पसंद नहीं। कहते हैं कि इनमें आप हमारी मां नहीं लगतीं। तुम्हीं बताओ क्या करूं?’’ (पृ.72) लेखन और समाजहित के कार्यों के संबंध में यही दमयंती आगे कहती है-‘‘बहन, यह काम तो यहीं धरे रह जाएंगे ओर कभी पूरे न होंगे। हमें आगे का भी सोचना है।’’ कितनी दिग्भ्रमित है दमयंती। जिसने अपने बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा किया। उन्हें सही और गलत का अर्थ समझाया। सही रास्ता दिखाया। जीवन का अर्थ समझाया। वहीं दमयंती वृद्धावस्था में आते ही अपने बच्चों के व्यवहार से इतनी भयाक्रांत हो गई कि उसने सही और गलत में भेद करना ही भुला दिया। परलोक के अस्तित्व के विचारों ने उसे इहलोक के उन दायित्वों से विमुख कर दिया जो अभी वह भली-भांति निभा सकती थी। अपितु ये कहा जाए कि यही वृद्धावस्था की दायित्वमुक्त आयु स्वयं को जीने की आयु होती है जिसे दमयंती जैसे व्यक्ति जीने का न तो साहस कर पाते हैं और न दसके बारे में सोच पाते हैं। परलोक के अस्तित्व की एक भेड़चाल या फिर वृद्धों को भयभीत कर रखने की वह चाल जिसमें उलझ कर वे युवाओं के जीवन में हस्तक्षेप न कर सकें।
आरण्या परलोक-भय की भेड़चाल से परे अपने रास्ते पर चल रही है। वह अपने तयशुदा दायित्वों के प्रति न केवल सजग है अपितु उन्हें निष्ठापूर्वक पूरे भी करना चाहती है। आयु को ले कर ईशान के ऊहापोह के उत्तर में आरण्या कहती है-‘‘मैं अपने को उम्र में इतना बड़ा महसूस नहीं करती जितना आप मान रहे हैं। मेरे आसपास मेरा परिवार नहीं फैला हुआ कि मैं अपने में मंा, नानी, दादी की बूढ़ी छवि ही देखने लगूं। ईशान, मुझे मेरा अपनापन निरंतरता का अहसास देता है।’’ (पृ.80) यही तो वह तथ्य है कि आयु को अनुभव करना ही आयु को से समझौता कर लेना है। आरण्या को यह समझौता स्वीकार नहीं है। वह बड़ी-बूढ़ी छवियों में उलझ कर स्वयं को बूढ़ी मान कर थकाना नहीं चाहती है। क्योंकि वह जानती है कि एकाकीपन उन रिश्तों की बूढ़ी छवियों के बीच और अधिक गहरा जाता है।
कथानक भले ही एकाकी वृद्धों के जीवन पर केन्द्रित हो किन्तु देश के बंटवारे का दर्द ‘समय सरगम’ में भी अपनी सम्पूर्णता के साथ दिखाई पड़ता है। ‘‘नई पुरानी दिल्ली अपनी घनी सजीली छब में हर हाल में अपनी सूरत और सीरत सम्हाले रहती। आज़ादी के साथ ही राजधानी में बाढ़ की तरह रेला उठ आया। आक्रामक विस्थापितों के ठट्ठ के ठट्ठ। यहां-वहां सब जगह। शहर के हर इलाके में। दिल्ली निवासी शरणार्थियों की भीड़ से परेशान और गंाव-कस्बों और शहरों से उखड़े हुए आक्रामक शरणार्थी-दिल्ली के सुसंस्कृत मिज़ाज में घूल भरी आंधियां चलने लगीं।’’ (पृ.43)
शरणार्थी अपने और अपनों के जीवन के लिए आक्रामक मुद्रा में भले ही थे किन्तु अधिकांश ऐसे थे जो अकेले रह गए थे। अतः अकेलेपन की चर्चा के समय देश के बंटवारे के दौरान उपजा अकेलापन भी विषयानुकूल है। पहले भरपूरा परिवार पारम्परिक और संस्कृति से ओतप्रोत फिर एक लम्बा अकेला जीवन। यह बंटवारे के समय परिस्थिति का परिणाम रहा किन्तु वर्तमान में यह प्रारब्ध बन गया है। दिल्ली जैसे महानगरों की गंगनचुम्बी इमारतों के छोटे-छोटे फ्लैट्स में एकल परिवार और अकेले बूढ़ों की वो दुनिया बस गई है जिनके बीच स्नेह की बेल सूख चुकी है। आरण्या और ईशान संयुक्त परिवार की अवधारणा के समाप्त होने पर चर्चा करते हैं तो आरण्या बोल उठती है-‘‘ईशान, मुझे संयुक्त परिवार का अनुभव नहीं। दूर-पास से जो इसकी आवाज़ें सुनीं वह सुखकर नहीं थीं। इतना जानती हूं कि परिवार की सुव्यवस्थित अस्मिता ओर गरिमा का मूल्य भी उनहें ही चुकाना होता है जिनका खाता दुबला हो। परिवार की सांझी श्री पैसे के व्यापारिक प्रबंधन में निहित है। उसकी आंतरिक शक्ति क्षीण हो चुकी है। घनी छांह की जगह घिसी हुई पुरानी चिन्दियां फरफरा रही हैं। जानती हूं ईशान, आपको यह बात ठीक नहीं लग रही, पर मैं अपनी कीमत पर इसकी पड़ताल कर रही हूं और ‘सत्य’ के नाना-रूप में संचारित छोटे-बड़े झूठ और झूठों से बनाए गए स्वर्णिम सत्यों की ठोंक-पीट ही इस सात्विक संसार की प्रेरणा है।’’ (पृ.64)
यदि वृद्धावस्था आ गई है तो क्या चैबीस घंटे ईश्वर की स्तुति एवं धर्म-दर्शन में व्यतीत करना चाहिए? ईशान आरण्या का परिचय दमयंती से कराता है। वह भी उनकी हमउम्र है। किन्तु वह इन दोनों की भांति एकाकी नहीं है वरन् अपने बेटों-बहुओं के साथ रह रही है। उसने समाज एवं परिवार की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप स्वयं को एक गुरु की शिष्या बना कर सत्संग के हवाले कर दिया है। ऊपर से देखने से यही लगता है कि वह अपनी इस स्थिति से प्रसन्न एवं संतुष्ट है। वास्तविकता इससे परे है। दमयंती का खान-पान गुरू के निर्देशानुसार बदल चुका है। पहनावा भी उन्हीं के अनुसार अपना लिया है। लेकिन बेटे, बहू फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। दमयंती मानो किसी भुलावे में जी रही है। वह कहती है-‘‘आरण्या, मैं सूती कपड़ा तन को छुआती न थी। एक दिन सत्संग के बाद मेरी गुरूजी ने टोक दिया। अब सूफियाने-से सूती जोड़े बनवाए हैं। मेरे बेटों और बहुओं की सुनो। रेशम पहनो तो कहते हैं, इस उम्र में ये मचक-दमक अच्छी नहीं लगती। सूती पहनूं तो वह भी पसंद नहीं। कहते हैं कि इनमें आप हमारी मां नहीं लगतीं। तुम्हीं बताओ क्या करूं?’’ (पृ.72) लेखन और समाजहित के कार्यों के संबंध में यही दमयंती आगे कहती है-‘‘बहन, यह काम तो यहीं धरे रह जाएंगे ओर कभी पूरे न होंगे। हमें आगे का भी सोचना है।’’ कितनी दिग्भ्रमित है दमयंती। जिसने अपने बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा किया। उन्हें सही और गलत का अर्थ समझाया। सही रास्ता दिखाया। जीवन का अर्थ समझाया। वहीं दमयंती वृद्धावस्था में आते ही अपने बच्चों के व्यवहार से इतनी भयाक्रांत हो गई कि उसने सही और गलत में भेद करना ही भुला दिया। परलोक के अस्तित्व के विचारों ने उसे इहलोक के उन दायित्वों से विमुख कर दिया जो अभी वह भली-भांति निभा सकती थी। अपितु ये कहा जाए कि यही वृद्धावस्था की दायित्वमुक्त आयु स्वयं को जीने की आयु होती है जिसे दमयंती जैसे व्यक्ति जीने का न तो साहस कर पाते हैं और न दसके बारे में सोच पाते हैं। परलोक के अस्तित्व की एक भेड़चाल या फिर वृद्धों को भयभीत कर रखने की वह चाल जिसमें उलझ कर वे युवाओं के जीवन में हस्तक्षेप न कर सकें।
आरण्या परलोक-भय की भेड़चाल से परे अपने रास्ते पर चल रही है। वह अपने तयशुदा दायित्वों के प्रति न केवल सजग है अपितु उन्हें निष्ठापूर्वक पूरे भी करना चाहती है। आयु को ले कर ईशान के ऊहापोह के उत्तर में आरण्या कहती है-‘‘मैं अपने को उम्र में इतना बड़ा महसूस नहीं करती जितना आप मान रहे हैं। मेरे आसपास मेरा परिवार नहीं फैला हुआ कि मैं अपने में मंा, नानी, दादी की बूढ़ी छवि ही देखने लगूं। ईशान, मुझे मेरा अपनापन निरंतरता का अहसास देता है।’’ (पृ.80) यही तो वह तथ्य है कि आयु को अनुभव करना ही आयु को से समझौता कर लेना है। आरण्या को यह समझौता स्वीकार नहीं है। वह बड़ी-बूढ़ी छवियों में उलझ कर स्वयं को बूढ़ी मान कर थकाना नहीं चाहती है। क्योंकि वह जानती है कि एकाकीपन उन रिश्तों की बूढ़ी छवियों के बीच और अधिक गहरा जाता है।
रिश्तों के एकाकीपन के तारतम्य में उषा प्रियंवदा की कहानी ‘वापसी’ सहसा स्मरण हो आती है। एक व्यक्ति जब रिटायर हो कर घर लौटता है तो घर में खलबली मच जाती है। उसे सदा के लिए कोई अपने बीच नहीं पाना चाहता है। घर का प्रत्येक सदस्य, यहां तक कि उसकी पत्नी भी चाहती है कि वह उसकी तरह समझौतावादी बन कर रहे अथवा फिर कहीं चला जाए। उसकी घर वापसी उसके घरवालों के लिए ही खटकने वाली हो जाती है। यही है अपनों के बीच का परायापन जो सेवानिवृत्त व्यक्ति को अकेला कर देता है। ईशान इसी अकेलेपन को जी रहा है। किन्तु आरण्या नहीं। आरण्या मंा, नानी, दादी नहीं बल्कि एक स्वावलम्बी स्त्री के रूप में जीवन जी रही है, वृद्धावस्था के फेंटे में आने के बावजूद भी। वह उन लोगों जैसी समझौतावादी नहीं है जो स्वयं को अशक्त मान लेते हैं और बहू-बेटों के तिरस्कार में भी अपने सुखों की तलाश करते शेष जीवन बिता देते हैं। बहुमंजिला इमारत में अपने फ्लैट (जो उनका अपना नहीं रहा, बहुओं-बेटों का हो चुका ) के ठीक बाहर सड़क के उस पार बने नन्हें से पार्क में उनकी दुनिया सिमट कर रह जाती है। वे यही सोच कर स्वयं को ढाढस बंधाते हैं कि ‘‘कामकाज से छुट्टी पा इसे भोगना भी सुख है जीने का। बहू-बेटों की नज़रों में रुखाई, अवज्ञा, उदासीनता कुछ भी दीखती रहे-परिवार के साथ हाने का सुख है गहरा। रहती है आत्मा शांत कि सभी कोई पास हैं। अपने साथ हैं।.....यह बात अलग है कि परिवारों में बड़े-बूढ़ों के अधिकार कमतर और ‘हां’ ‘न’ का संकोच ज्यादा है। पीढ़ी सरक जाए तो अख्तियार खुद ही आधे-पौने हो जाते हैं। बहू -बेटों की मरजी मुताबिक चलना। वे जैसा चाहें रहते रहें। हम क्यों तानाशाह बने हुक्म चलाते रहें।’’ (पृ.89-90) अपनी स्थिति को नियति मान लेना और अपने बहू-बेटों के अनुरूप स्वयं को ढाल लेना इतना भी बुरा नहीं है जितना कि रिश्तेदारों के होते हुए भी अकेले पड़ जाना। ईशान की परिचित कामिनी इसी विडम्बना को जी रही है। कामिनी का भाई अपने परिवार के साथ अलग रहता है। कामिनी की सेवा-टहल के लिए ‘खूकू’ नाम की नौकरानी है। नौकरानी भी ऐसी जो कामिनी की अवस्था से तादात्म्य नहीं बिठा सकी है। वह आलमारी की चाबी के बारे में पूछने पर ईशान से कहती है-‘‘कभी मेम साहिब के पास होती है, कभी मेरे पास। उन्हें कुछ याद नहीं रहता। कहीं रख देती हैं और मुझ पर बरसने लगती हैं। क्या करूं साहिब, मुझे ऐसी नौकरी छोड़ देनी चाहिए पर इनकी हालत पर तरस आता है।’’ (पृ.99) ईशान और आरण्या दोनों समझ जाते हैं कि यह ‘तरस’ वास्तविक ‘तरस’ नहीं है। इसके पीछे निहित स्वार्थ की गंध उन्होंने स्पष्ट महसूस की। किन्तु वे उस लाचार वृद्धा के रिश्तेदार नहीं हैं जो कोई ठोस कानूनी क़दम उठा सकें। जो रिश्तेदार है अर्थात् कामिनी का भाई उसे अपनी बहन से अधिक अपनी बहन के घर से प्यार है। कामिनी ईशान और आरण्या को बताती है कि ‘‘मुझे दलाल बता गया है कि भाई ने मेरे घर का सौदा कर लिया है। बयाना ले चुका है। खूकू ने मुझे नहीं बताया पर बिल्डर घर को दो बार आगे-पीछे और अंदर से देख गया है। मैं तब सोई पड़ी थी।’’ कामिनी आगे बताती है कि ‘‘एक रात देखा तो मेरी डाक्यूमेंट फाईल में घर के पेपर नहीं थे। अगली रात यह (खूकू) बाहर ताला डाल कर चली गई तो फिर आलमारी खोली। सब खाने छान मारे फाईल खोली तो असली की जगह फोटोस्टेट काॅपी रखी थी।....असली अब मेरे पास नहीं है।’’ (पृ. 98) यह छल, वह भी अपने सगे भाई और अपनी नौकरानी के हाथों। कामिनी को यह सब सहन करना पड़ रहा था। क्यश एक वृद्धा के लिए जिसने अपना जीवन शान से सिर उठा कर, निद्र्वन्द्व हो कर जिया हो, आसान हो सकता था? कामिनी के लिए कुछ भी आसान नहीं था।
आरण्या के अपने अनुभव भी कम कटु नहीं थे। यदि वृद्ध व्यक्ति अकेला हो तो क्या उसे सुगमता से किराए का घर मिल सकता है? वह न तो युवाओं जैसी पार्टियां करेगा, न तो लड़कियों अथवा लड़कों को अपने घर लाएगा, युवाओं में प्रचलित कोई भी असमाजिक हरकत नहीं करेगा चाहे वह वृद्ध हो या वृद्धा। फिर तो मकान मालिक को ऐसे वृद्धों को किराए से मकान देने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति से सुरक्षित वृद्ध का तो और पहले स्वागत किया जाना चाहिए। किन्तु इस सिक्के का दूसरा पहलू अत्यंत भयावह है। आरण्या को मकान बदलने की नौबत आती हैं वह एक अदद किराए का मकान ढूंढने निकल पड़ती है।
‘‘एक अच्छे खासे घर को दो-तीन बार देख कर उसका एडवांस देना चाहा तो ऐजेंट के साथ खड़े बुजुर्ग ने पूछा-यह बताएं कि आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
जिम्मेदारी? क्या मतलग?
आप अकेली रहेंगी कि कोई और भी साथ में होगा?
मैं रहूंगी और मैं ही अपने लिए जिम्मेदार हूं।
आपकी जन्म तारीख किस सन् की है?
यह क्यों पूछ रहे हैं आप? इसलिए कि हमें पूछना चाहिए। कल को चली-चलाई को कुछ चक्कर हो तो हम झमेले में क्यों पड़ें।’’ (पृ. 122)
आरण्या के अपने अनुभव भी कम कटु नहीं थे। यदि वृद्ध व्यक्ति अकेला हो तो क्या उसे सुगमता से किराए का घर मिल सकता है? वह न तो युवाओं जैसी पार्टियां करेगा, न तो लड़कियों अथवा लड़कों को अपने घर लाएगा, युवाओं में प्रचलित कोई भी असमाजिक हरकत नहीं करेगा चाहे वह वृद्ध हो या वृद्धा। फिर तो मकान मालिक को ऐसे वृद्धों को किराए से मकान देने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति से सुरक्षित वृद्ध का तो और पहले स्वागत किया जाना चाहिए। किन्तु इस सिक्के का दूसरा पहलू अत्यंत भयावह है। आरण्या को मकान बदलने की नौबत आती हैं वह एक अदद किराए का मकान ढूंढने निकल पड़ती है।
‘‘एक अच्छे खासे घर को दो-तीन बार देख कर उसका एडवांस देना चाहा तो ऐजेंट के साथ खड़े बुजुर्ग ने पूछा-यह बताएं कि आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
जिम्मेदारी? क्या मतलग?
आप अकेली रहेंगी कि कोई और भी साथ में होगा?
मैं रहूंगी और मैं ही अपने लिए जिम्मेदार हूं।
आपकी जन्म तारीख किस सन् की है?
यह क्यों पूछ रहे हैं आप? इसलिए कि हमें पूछना चाहिए। कल को चली-चलाई को कुछ चक्कर हो तो हम झमेले में क्यों पड़ें।’’ (पृ. 122)
यानी मृत्यु का आकलन करके मकान किराए पर देना तय करना। एकदम अमानवीय विचार। एकदम अमानवीय कृत्य। किन्तु यही सामाजिक सत्य है, घिनौना, स्वाभाविक सोच से परे। मृत्यु वृद्धावस्था की सगी-संगिनी हो, यह आवश्यक नहीं है। यह आयु का उतार चढ़ाव नहीं देखती है। बस, अपने मतलब की संासें गिनती है और आ धमकती है। शिशु भी युवा भी, वृद्ध भी सभी इसी की छांह में सांसे लेते हैं। यदि पल भर को मान लिया जाए कि मृत्यु और वृद्धावस्था सगी बहनें हैं तो ऐसी दशा में तो वृद्ध को सहारा और सिर पर छत मिलनी ही चाहिए। किन्तु स्वार्थ और आर्थिक लोभ इंसान को पाषाणहृदय बना देता है। तभी तो जब एक अन्य फ्लैट को तय करने के लिए आरण्या एजेंट से बातचीत करती है।
‘‘एजेंट ने कंपनी लीज़ की मांग की।
कुछ देर सोचती रही फिर हामी भरी। हां, दे सकूंगी।
नाम बताइए कंपनी का। कौन है?
मेरे प्रकाशक हैं।
क्या आप लेखक हैं! किताबें लिखती हैं? ऐसा है तो कहां से ला कर देंगी किराया?
आरण्या बिना जबाव दिए नीचे उतर गई।’’ (पृ. 122)
कृष्णा सोबती यहां एक साथ दो बिन्दुओं पर प्रहार करती हैं। एक तो वृद्धों के प्रति मकानमालिक और ऐजेंट के मानवतारहित व्यवहार पर और दूसरा भारत में लेखकों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा पर। भारत में आदिकाल से लेखन को चैंसठ कलाओं में से एक कला माना जाता रहा है। किन्तु मान्यता और यथार्थ के बीच की गहरी खाई यहां हमेशा रही है। राजाओं के जमाने में राजाश्रय पा जाने वाले साहित्यकार अर्थ और समाज से प्रतिष्ठित रहते थे जबकि राजाश्रयविहीन साहित्यकार यदि पूछ ेभी जाते रहे हैं तो अपनी मृत्यु के सदियों बाद। आधुनिक युग में भी यही स्थिति है। पाश्चात्य जगत में ऐसा नहीं है। वहां साहित्यकार सिर्फ साहित्य सृजन कर के रायल्टी के दम पर अपनी रोजी-रोटी चला सकता है। किन्तु भारत में नहीं। यहां लेखक को बुद्धिजीवी की श्रेणी में भले ही गिना जाए परन्तु उसकी ‘लक्ष्मीप्रिया’ नहीं मानी जाती है। जो बुद्धि सीधे धनार्जन में लगे उसकी साख है, साहित्य में लगने वाली बुद्धि की नहीं। साहित्य का ‘मार्केट वेल्यू’ साहित्य व्यवसायी के लिए भले हो पर साहित्यकार के लिए नहीं होता है। अस्तु एक साहित्यकार की आर्थिक साख और उसके साहित्य के बल पर उसके जीवन की मूल्यवत्ता होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।
आरण्या को अपनी सहेली के घर शरण लेनी पड़ती है। तब ईशान के मन में आता है कि क्यों न आरण्या उसके घर में आ कर रहे एक साथी की तरह। आरण्या कुछ हिचकते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। दो वृद्धजन परस्पर एक-दूसरे का सहारा बन कर जीने लगते हैं। विपरीत लिंगी होते हुए भी एक वासना रहित जीवन। विशुद्ध मैत्री पर आधारित साथ जिसमें एक-दूसरे का सुख-दुख, चिन्ता, आवश्यकताएं और पूरकता निहित है। ‘‘कितने बरस गुज़र गए। हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। कहां मालूम था िकपतझर के इस मौसम में हम लोग मिल जाएंगे, पुराने परिचितों की तरह नहीं-नए मित्रों की तरह। लंबा अरसा हो गया है इस शहर में रहते। अपने-अपने खातों को देंखें तो कहां जान पाएंगे कि कितना खोया और कितना पाया। हां, आरण्या, तुम्हें जान लेने पर यह तो लगता है कि जीना बैंक का अकाउंट नंबर नहीं, जिसका कुल जोड़ कुछ आंकड़ों में हो। मैं अब किसी असमंजस में नहीं हूं। क्यों न अपने जाने को सहज-सरल कर लें। हम दोनों में से किसी को दिक्कत न होगी।’’ (पृ.147)
‘‘एजेंट ने कंपनी लीज़ की मांग की।
कुछ देर सोचती रही फिर हामी भरी। हां, दे सकूंगी।
नाम बताइए कंपनी का। कौन है?
मेरे प्रकाशक हैं।
क्या आप लेखक हैं! किताबें लिखती हैं? ऐसा है तो कहां से ला कर देंगी किराया?
आरण्या बिना जबाव दिए नीचे उतर गई।’’ (पृ. 122)
कृष्णा सोबती यहां एक साथ दो बिन्दुओं पर प्रहार करती हैं। एक तो वृद्धों के प्रति मकानमालिक और ऐजेंट के मानवतारहित व्यवहार पर और दूसरा भारत में लेखकों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा पर। भारत में आदिकाल से लेखन को चैंसठ कलाओं में से एक कला माना जाता रहा है। किन्तु मान्यता और यथार्थ के बीच की गहरी खाई यहां हमेशा रही है। राजाओं के जमाने में राजाश्रय पा जाने वाले साहित्यकार अर्थ और समाज से प्रतिष्ठित रहते थे जबकि राजाश्रयविहीन साहित्यकार यदि पूछ ेभी जाते रहे हैं तो अपनी मृत्यु के सदियों बाद। आधुनिक युग में भी यही स्थिति है। पाश्चात्य जगत में ऐसा नहीं है। वहां साहित्यकार सिर्फ साहित्य सृजन कर के रायल्टी के दम पर अपनी रोजी-रोटी चला सकता है। किन्तु भारत में नहीं। यहां लेखक को बुद्धिजीवी की श्रेणी में भले ही गिना जाए परन्तु उसकी ‘लक्ष्मीप्रिया’ नहीं मानी जाती है। जो बुद्धि सीधे धनार्जन में लगे उसकी साख है, साहित्य में लगने वाली बुद्धि की नहीं। साहित्य का ‘मार्केट वेल्यू’ साहित्य व्यवसायी के लिए भले हो पर साहित्यकार के लिए नहीं होता है। अस्तु एक साहित्यकार की आर्थिक साख और उसके साहित्य के बल पर उसके जीवन की मूल्यवत्ता होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।
आरण्या को अपनी सहेली के घर शरण लेनी पड़ती है। तब ईशान के मन में आता है कि क्यों न आरण्या उसके घर में आ कर रहे एक साथी की तरह। आरण्या कुछ हिचकते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। दो वृद्धजन परस्पर एक-दूसरे का सहारा बन कर जीने लगते हैं। विपरीत लिंगी होते हुए भी एक वासना रहित जीवन। विशुद्ध मैत्री पर आधारित साथ जिसमें एक-दूसरे का सुख-दुख, चिन्ता, आवश्यकताएं और पूरकता निहित है। ‘‘कितने बरस गुज़र गए। हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। कहां मालूम था िकपतझर के इस मौसम में हम लोग मिल जाएंगे, पुराने परिचितों की तरह नहीं-नए मित्रों की तरह। लंबा अरसा हो गया है इस शहर में रहते। अपने-अपने खातों को देंखें तो कहां जान पाएंगे कि कितना खोया और कितना पाया। हां, आरण्या, तुम्हें जान लेने पर यह तो लगता है कि जीना बैंक का अकाउंट नंबर नहीं, जिसका कुल जोड़ कुछ आंकड़ों में हो। मैं अब किसी असमंजस में नहीं हूं। क्यों न अपने जाने को सहज-सरल कर लें। हम दोनों में से किसी को दिक्कत न होगी।’’ (पृ.147)
जीवन से एक साझापन ही आयु के समय को आसान बना सकता है बशर्ते यह साझापन विवशता का नहीं सहजता और उत्फुल्लता का हो। अन्यथा एकाकी वृद्धों के पास अपनी बचीखुची सांसें गिनते हुए दिन काटने के सिवा कोई चारा नहीं बचता है। एक ओर कामिनी, दमयंती जैसे वृद्ध हैं जो पारिवारिक दबाव के चलते आयु के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं या फिर एक निःश्वास की भांति मंथर गति से घिसटते रहते हैं मृत्यु की ओर। ईशान जैसे वृद्ध व्यक्ति भी हैं जो परिस्थितियों को एक मध्यममार्गी की भांति स्वीकार करते हैं। वहीं आरण्या जैसे वृद्ध हैं जो बिना किसी को कष्ट पहुंचाए अपना जीवन अपने ढंग से जीने के लिए कृतसंकल्प रहते हैं। स्वावलंबी और स्वाभिमानी ढंग से। यद्यपि ऐसे मार्ग में अवरोध ही अवरोध हैं। एक तो स्त्री, वह भी अकेली और उस पर लेखिका। न कोई आर्थिक साख, न कोई सामाजिक सहारा। फिर भी अडिग रह कर जीवन के शेष दिनों को अपनी इच्छानुरुप ढालने का साहस। यही साहस उसे ईशान की निर्विकार मित्रता उपलब्ध कराता है। कृष्णा सोबती ‘समय सरगम’ में इसी सत्य को बखूबी सामने रखती हैं कि जीवन उतार-चढ़ावों से परिपूर्ण है। यदि तार-स्वर हैं तो मंद-स्वर भी हैं। फिर भी ये सभी एक रागों में निबंद्ध हैं।
‘समय सरगम’ की भाषा पाठक से सीधा संवाद करती है। अपनी भाषा के संदर्भ में एक साक्षात्कार में कृष्णा सोबती ने कहा था कि-‘‘ पात्र की सामाजिकता, उसका सांस्कृतिक पर्यावरण उसके कथ्य की भाषा को तय करते हैं। उसके व्यक्तित्व के निजत्व को, मानवीय अस्मिता को छूने और पहचानने के काम लेखक के जिम्मे हैं। भाषा वाहक है उस आंतरिक की जो अपनी रचनात्मक सीमाओं से ऊपर उठकर पात्रों के विचार स्रोत तक पहुंचता है। सच तो यह है कि किसी भी टेक्स्ट की लय को बांधने वाली विचार-अभिव्यक्ति को लेखक को सिर्फ जानना ही नहीं होता, गहरे तक उसकी पहचान भी करनी होती है। अपने से होकर दूसरे संवेदन को समझने और ग्रहण करने की समझ भी जुटानी होती है। एक भाषा वह होती है जो हमने मां-बोली की तरह परिवार से सीखी है- एक वह जो हमने लिखित ज्ञान से हासिल की है। और एक वह जो हमने अपने समय के घटित अनुभव से अर्जित की है। जिस लयात्मकता की बात आपने की, समय को सहेजती और उसे मौलिक स्वरूप देती वैचारिक अंतरंगता का मूल इसी से विस्तार पाता है।’’ उनकी भाषा की यही विशेषता कृष्णा जी के सृजन में आत्मीयता पैदा करती है। इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उनका कथानक जो ‘समय सरगम’ में ढल कर समाज में वृद्धों की दशा को खंगालता है, महसूस कराता है।
‘समय सरगम’ की भाषा पाठक से सीधा संवाद करती है। अपनी भाषा के संदर्भ में एक साक्षात्कार में कृष्णा सोबती ने कहा था कि-‘‘ पात्र की सामाजिकता, उसका सांस्कृतिक पर्यावरण उसके कथ्य की भाषा को तय करते हैं। उसके व्यक्तित्व के निजत्व को, मानवीय अस्मिता को छूने और पहचानने के काम लेखक के जिम्मे हैं। भाषा वाहक है उस आंतरिक की जो अपनी रचनात्मक सीमाओं से ऊपर उठकर पात्रों के विचार स्रोत तक पहुंचता है। सच तो यह है कि किसी भी टेक्स्ट की लय को बांधने वाली विचार-अभिव्यक्ति को लेखक को सिर्फ जानना ही नहीं होता, गहरे तक उसकी पहचान भी करनी होती है। अपने से होकर दूसरे संवेदन को समझने और ग्रहण करने की समझ भी जुटानी होती है। एक भाषा वह होती है जो हमने मां-बोली की तरह परिवार से सीखी है- एक वह जो हमने लिखित ज्ञान से हासिल की है। और एक वह जो हमने अपने समय के घटित अनुभव से अर्जित की है। जिस लयात्मकता की बात आपने की, समय को सहेजती और उसे मौलिक स्वरूप देती वैचारिक अंतरंगता का मूल इसी से विस्तार पाता है।’’ उनकी भाषा की यही विशेषता कृष्णा जी के सृजन में आत्मीयता पैदा करती है। इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उनका कथानक जो ‘समय सरगम’ में ढल कर समाज में वृद्धों की दशा को खंगालता है, महसूस कराता है।
निष्कर्ष
‘समय सरगम’ कृष्णा सोबती का एक ऐसा उपन्यास है जो वृद्धावस्था को प्राप्त एकाकी रह रहे स्त्री-पुरुष के विचारों, इच्छाओं, परिस्थितियों एवं हर ओर से मिलने वाली उपेक्षा व अवहेलना का मनोसामाजिक विश्लेषण करता है। यह उपन्यास वृद्धविमर्श का एक ऐसा धरातल तैयार करता है जिस पर खड़े हो गया वृद्धावस्था के कम्पन को सूक्ष्मा से अनुभव किया जा सकता है। संवेदनाओं एवं दृढ़ता की प्रचुरता को रेखांकित करने के साथ ही यह समाज से आग्रह करता है कि वृद्धों के प्रति अपने दृष्टिकोण में सुधार लाने की आवश्यकता है। वस्तुतः ‘समय सरगम’ एक सशक्त मनोसामाजिक उपन्यास है।
-------------------------
संदर्भ:
1. समय सरगम, कृष्णा सोबती, राजकमल प्रकाशन, सन 2008, पेपर बैक।
2. लेख, समाज में वृद्धों की दशा को खंगालता समय सरगम, लेखिका- डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह, सापेक्ष 60 (कृष्णा सोबती के कृतित्व पर केन्द्रित), संपादक- महावीर अग्रवाल,प्रकाशक- सापेक्ष, ए-14, आदर्श नगर, दुर्ग (छ.ग.)
3. सापेक्ष 60 (कृष्णा सोबती के कृतित्व पर केन्द्रित), संपादक- महावीर अग्रवाल,प्रकाशक- सापेक्ष, ए-14, आदर्श नगर, दुर्ग (छ.ग.)
4. कृष्णा सोबती के कृतित्व पर केन्द्रित एक अनूठी पुस्तक ‘‘सापेक्ष 60’’, पुस्तक समीक्षा, समीक्षक - डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह, दैनिक ‘‘आचरण’’ सांगर संस्करण, 14.12.2012
---------------------------------
- डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह
‘समय सरगम’ कृष्णा सोबती का एक ऐसा उपन्यास है जो वृद्धावस्था को प्राप्त एकाकी रह रहे स्त्री-पुरुष के विचारों, इच्छाओं, परिस्थितियों एवं हर ओर से मिलने वाली उपेक्षा व अवहेलना का मनोसामाजिक विश्लेषण करता है। यह उपन्यास वृद्धविमर्श का एक ऐसा धरातल तैयार करता है जिस पर खड़े हो गया वृद्धावस्था के कम्पन को सूक्ष्मा से अनुभव किया जा सकता है। संवेदनाओं एवं दृढ़ता की प्रचुरता को रेखांकित करने के साथ ही यह समाज से आग्रह करता है कि वृद्धों के प्रति अपने दृष्टिकोण में सुधार लाने की आवश्यकता है। वस्तुतः ‘समय सरगम’ एक सशक्त मनोसामाजिक उपन्यास है।
-------------------------
संदर्भ:
1. समय सरगम, कृष्णा सोबती, राजकमल प्रकाशन, सन 2008, पेपर बैक।
2. लेख, समाज में वृद्धों की दशा को खंगालता समय सरगम, लेखिका- डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह, सापेक्ष 60 (कृष्णा सोबती के कृतित्व पर केन्द्रित), संपादक- महावीर अग्रवाल,प्रकाशक- सापेक्ष, ए-14, आदर्श नगर, दुर्ग (छ.ग.)
3. सापेक्ष 60 (कृष्णा सोबती के कृतित्व पर केन्द्रित), संपादक- महावीर अग्रवाल,प्रकाशक- सापेक्ष, ए-14, आदर्श नगर, दुर्ग (छ.ग.)
4. कृष्णा सोबती के कृतित्व पर केन्द्रित एक अनूठी पुस्तक ‘‘सापेक्ष 60’’, पुस्तक समीक्षा, समीक्षक - डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह, दैनिक ‘‘आचरण’’ सांगर संस्करण, 14.12.2012
------------------------------
- डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह
---------------------------------