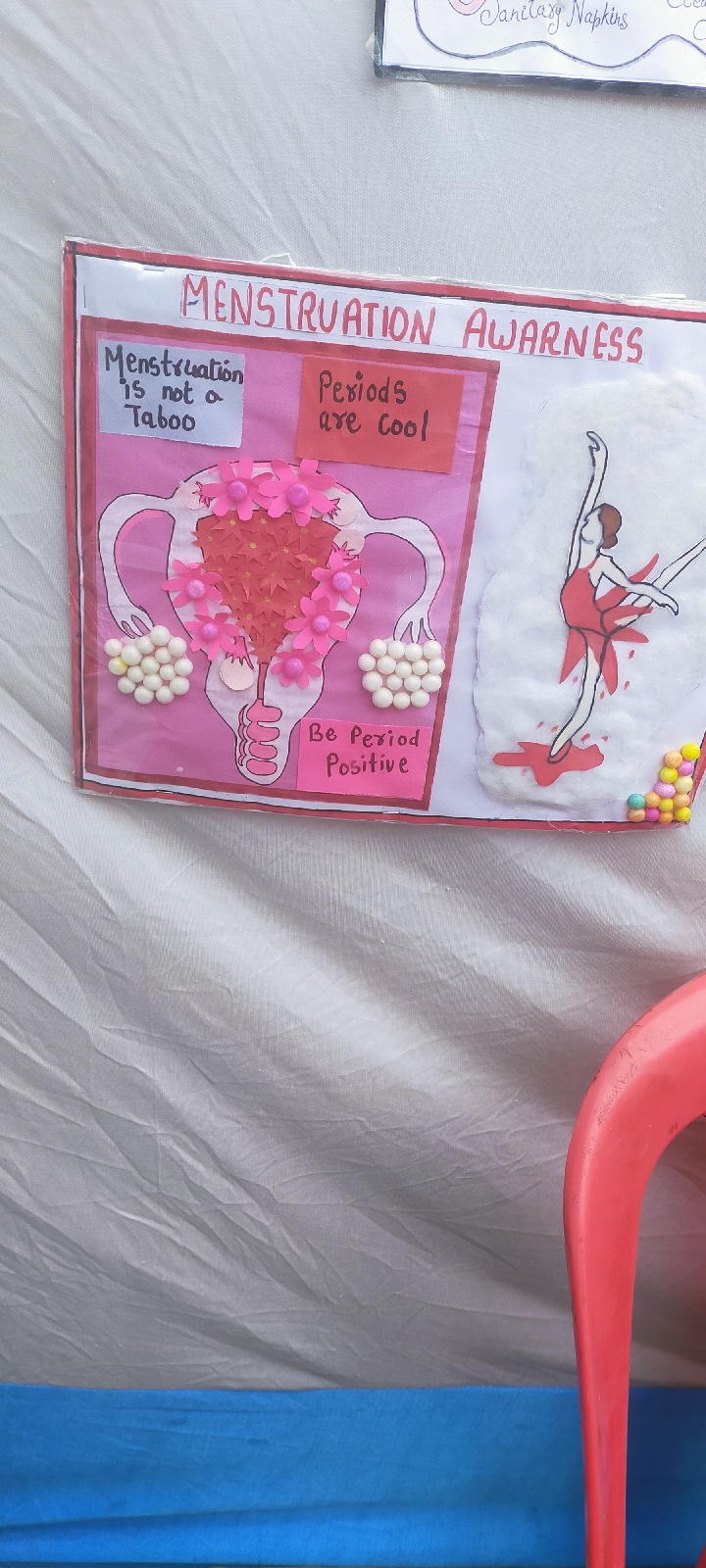दैनिक 'नयादौर' में मेरा कॉलम
शून्यकाल
पहाड़ कोठी, मदार साहब और हनुमानजी
- डॉ (सुश्री) शरद सिंह
. स्मृतियां जीवन की अमूल्य निधि होती हैं। स्मृतियों में वह अतीत समाया होता है जो व्यक्ति की निजी थाती तो होता ही है साथ ही यदि उसे लेखबद्ध कर के पढ़ा जाए तो तत्कालीन पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक इतिहास बन जाता है। उस समय उसमें संबंधित व्यक्ति गौण हो जाता है और तत्कालीन घटनाएं एवं दशाएं प्रमुखता से मुखर हो उठती हैं। बिलकुल मुझे ऐसा ही लगता है जब मैं अपनी स्मृतियों को लेखबद्ध करती हूं।
शहद से मीठे और पके आम जैसे रसीले बचपन के दिनों की सुनहरी आभा आज भी स्मृतियों की देहरी पर दमकती रहती है। बड़े ही खूबसूरत दिन थे। तब पहाड़ बहुत ऊंचे लगते थे और तालाब बहुत गहरे। हनुमान जी तब वैसे हनुमान जी नहीं लगते थे, जैसे अब लगते हैं। जी हां, मैं उसी पन्ना की बात कर रही हूं, वही शहर जहां मेरा बचपन व्यतीत हुआ। जहां मेरा घर था, वह हिरणबाग कहलाता था। यह कहा जाता था कि राजशाही के समय उस परिसर में हिरण पाले जाते थे। उस परिसर में आम, नीम वट और पीपल के अलावा नींबू, चांदनी, बगनविलास के पेड़ भी थे। जिनमें से कुछ धीरे-धीरे कटते चले गए और बाद में आम, नीम, वट जैसे बड़े वृक्ष ही बचे। उस परिसर में दो बड़े कुएं थे, जिनमें हमेशा पानी लबालब भरा रहता था। इतना स्वच्छ पानी कि आस-पास के मोहल्ले की महिलाएं वहां से पीने का पानी भर कर ले जाया करती थीं। जब नाना जी से कोई कहानी सुनाते समय पनिहारिन का उल्लेख करते तो मेरे ज़ेहन में उन कुओं से पानी भरने वाली महिलाएं कौंध जातीं । फिर मेरे लिए कहानी की पनिहारिन की कल्पना करना आसान हो जाता । सीधे पल्ले की साड़ी, माथे तक घूंघट, कमर में चांदी की करधनी, हाथों में कांच की ढेर सारी चूड़ियां, सिर पर दो-दो घड़े और हाथों में लोहे की बाल्टियां। यानी ग़ज़ब का स्टेमिना। उनके घर से कुओं की दूरी कम से कम एक-दो किलोमीटर रहती ही थी। खूबसूरत ऊंची जगत वाले वे दोनों कुएं जिनमें पानी निकालने के लिए परंपरागत लकड़ी की घिर्रियां लगी हुई थीं ।
हिरणबाग परिसर के मुख्य द्वार पर लोहे का बड़ा-सा फाटक था जिस पर चढ़कर हम लोग झूला झूलते थे और डांट खाते थे। फाटक के बाहर चौराहा था। आज भी है। जिसका एक रास्ता छत्रसाल पार्क से होते हुए सिटी कोतवाली की तरफ जाता था। दूसरा रास्ता छोटे बाजार की ओर। दो रास्ते कुछ दूर समानांतर जाते थे जिनमें से एक रास्ता धर्म सागर तालाब की ओर जाता था और दूसरा पहाड़ कोठी की ओर ऊंचाई पर चढ़ता चला जाता था। पहाड़ कोठी नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां छोटा सा पहाड़ था जिस पर सरकारी कोठियां बनी हुई थीं। आज भी यथावत हैं। किंतु आज वह पहाड़ इतना बड़ा नहीं लगता है जितना बचपन में लगता था। आज वह पहाड़ इतना बड़ा रहा भी नहीं। बचपन के उस पहाड़ में अनेक वृक्ष थे। वह हरियाली से ढंका रहता था लेकिन आज उस पहाड़ की ढलान पर भी अनेक घर बन चुके हैं। पहाड़ कोठी की अपनी विशेषताएं थी। वहां एक्सक्यूटिव इंजीनियर, एक्साइज ऑफीसर तथा डीएफओ का बंगला था। सबसे बड़ा कलेक्टर का बंगला था। इसके अलावा कुछ और छोटे-छोटे बंगले थे जो एसडीओ आदि को एलॉट किए जाते थे। वहां सबसे बड़ा भवन सर्किट हाउस था। यह सारे भवन आज भी मौजूद हैं।
एक्सक्यूटिव इंजीनियर के आलीशान बंगले में एक कुंड (चौपड़ा) बना हुआ था। जो बहुत ही डरावना लगता था। जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तो तत्कालीन एक्सक्यूटिव इंजीनियर की बेटी मेरे साथ पढ़ती थी। अब मुझे उसका नाम तो स्मरण नहीं है किंतु वह बंगला ज़रूर याद है। हम दो-तीन बच्चे अपनी उस सहेली के पास खेलने जाया करते थे। मां से अनुमति लेते समय यह हर बार सुनने को मिलता था कि "ठीक है जाओ ! लेकिन कुंड की तरफ मत जाना। उस में झांकना भी मत। उससे दूर रहना।"
.. इतनी सारी हिदायतें देकर मां जाने की इजाजत देती थीं। वह वाकई बहुत गहरा कुंड था। उसमें कई सीढ़ियां थीं। उसकी गहराई का अंदाज़ा कम से कम उस समय तो नहीं लगाया जा सकता था। जाहिर है, मुझे उस कुंड से डर लगता था और मैं उसके पास जाने से हिचकती थी।
पीडब्ल्यूडी के एक्सक्यूटिव इंजीनियर के उस बंगले के सामने राजाओं के जमाने की पुरानी बड़ी-सी तोप की बैरल रखी हुई थी। हम लोग अक्सर उस पर बैठा करते थे। उस बैरल का मुंह शहर की ओर था। मानो वह शहर की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सदा कटिबद्ध हो । एक्सक्यूटिव इंजीनियर के बंगले से आगे आखरी बंगला डीएफओ का था। बहुत ही बड़ा-सा बंगला। जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। इन सभी बंगलों के सामने गार्ड्स पहरा देते थे। लेकिन हम बच्चों के लिए कहीं कोई रोक-टोक नहीं थी। उस समय बहुत ही सीधा सरल माहौल था। वे गार्ड्स भी हमसे हंसते मुस्कुराते मिलते थे और कभी कभी कुछ खाने को भी दे दिया करते थे। कभी चॉकलेट तो कभी कोई फल। तनिक भी डर या अविश्वास का माहौल नहीं था। हम लोग कभी-कभी सर्किट हाउस भी चले जाया करते थे। जब कोई अधिकारी वहां ठहरा नहीं रहता था और कमरे खाली पड़े रहते थे तो वहां के केयरटेकर हम बच्चों को कमरे में जाने की इजाजत दे दिया करते थे। लेकिन इस शर्त के साथ कि हम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी तरह की गंदगी नहीं फैलाएंगे। हमें उनकी सारी शर्तें मंजूर रहतीं। हम वहां दीवार पर लगे बड़े-बड़े दर्पणों में अपने आप को देखते और खुश होते। फिर बाहर आकर सर्किट हाउस के परिसर में कुछ देर खेलते और फिर लौट जाते। वहां से धर्म सागर तालाब भी दिखाई देता था। जोकि बहुत सुंदर दृश्य होता था।
डीएफओ के बंगले के आगे भी रास्ता था जो पहाड़ की चोटी तक जाता था। लेकिन बंगले के आगे का रास्ता कच्चा था। उस रास्ते में आगे चलकर एक मजार स्थापित थी जो "मदार साहब" कहलाती थी। निश्चित रूप से यह "मजार साहब" का ही अपभ्रंश थी। उस मजार पर हमेशा सुनहरे किनारों वाली हरे रंग की चादर चढ़ी रहती थी और वह पूरा क्षेत्र लोबान की सुगंध से महकता रहता था। हर शुक्रवार कोई न कोई मुस्लिम परिवार चादर चढ़ाने मदार साहब जाया करता था। पूरे बाजे गाजे के साथ। विशेष रूप से जिसकी मन्नत पूरी होती थी वह हाथठेले पर चादर और चढ़ावा रखवा कर और लाउडस्पीकर पर गाना बजाते हुए जुलूस के रूप में जाता था। उसमें परिवार की महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी शामिल रहते थे। लाउडस्पीकर पर हमेशा एक ही गाना बजाया जाता था जो वास्तव में ख्वाजा की इबादत में गाए जाने वाली कव्वाली थी। वह कव्वाली मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इसीलिए आज भी उसके बोल याद हैं -
"भर दो झोली मेरी या मोहम्मद
लौटकर मै न जाऊंगा खाली..."
अब तो इस कव्वाली हो अनेक कव्वालों द्वारा गाया जा चुका है। पर उस समय जो कव्वाली बजती थी वह शायद साबरी ब्रदर्स के द्वारा गाई गई थी।
मदार साहब की बहुत मान्यता थी। सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग वहां मन्नतें मांगने और चादर चढ़ाने जाया करते थे। मदार साहब से और ऊपर जाने पर पहाड़ की चोटी पर पहुंचते थे जो लगभग समतल स्थान था। वहां अनेक ध्वंसावशेष मौजूद थे जिनमें से एकाध तो इस प्रकार गोलाकार थे कि जिससे यह लगता था कि संभवत वहां कभी बौद्ध स्तूप रहा होगा। यद्यपि इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं हैं। किंतु यह असंभव भी नहीं है।
पहाड़ कोठी से नीचे उतरते समय घुमावदार रास्ता था। एक गहरा अंधा मोड़ और दूसरा खुला मोड़। दूसरे मोड़ पर हनुमान जी का मंदिर था। जोकि नीचे से ऊपर जाते समय पहले पड़ता था। पत्थर की फर्शी से ढंका हुआ बड़ा-सा आंगन। जो सड़क से 4-5 सीढ़ियां नीचे था । आंगन में एक ओर हनुमान जी की मढ़िया थी। उस मढ़िया की फटकी (छोटा दरवाजा) हमेशा खुली रहती थी। तीन ओर लोहे के सींखचे थे। उन दिनों न हनुमान जी को इंसानों का डर था और न इंसानों की नीयत में खोट थी कि वे वहां से कुछ चुराने का प्रयास करते। वैसे देखा जाए तो हनुमान जी की उस मढ़िया में चुराने लायक कुछ था ही नहीं। एक आदद पत्थर की मूर्ति थी जिसे पुजारी जी सुबह मुंह अंधेरे नहला-धुला कर, उस पर सिंदूर का लेप कर दिया करते थे। सिंदूर के लेप के ऊपर हनुमान जी के चेहरे पर बड़ी-बड़ी सुंदर दो आंखें चिपका दी जाती थीं। सुबह मंदिर में घंटे बजाकर पूजा की जाती और प्रसाद बांटा जाता। आमतौर पर नारियल और चिरौंजी दाने का। शाम को भी आरती और पूजा होती। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को वहां मेले जैसी भीड़ जुड़ती थी। अनेक श्रद्धालु शुद्ध मावे के पेड़े, बेसन के लड्डू या भोग के लड्डू (जो सिर्फ पूजा में चढ़ावे के लिए ही बनाए जाते थे इसीलिए उन्हें भोग के लड्डू कहा जाता था) चढ़ाते थे। साथ में नारियल भी। हनुमान जी को चढ़ाने के बाद शेष प्रसाद वहां उपस्थित बच्चों और बड़ों सभी में समान रूप से बांट दिया जाता था। अनेक बच्चे प्रसाद पाने के लालच में ही मंगलवार और शनिवार को मंदिर पहुंच जाया करते थे।
हनुमान जी का मंदिर मेरे घर से अधिक दूर नहीं था। कई बार मैं, वर्षा दीदी और कॉलोनी के अन्य बच्चे मंदिर प्रांगण में खेलने चले जाया करते थे। मंदिर प्रांगण में एक चिल्ली का वृक्ष था। उस वृक्ष में गर्मी के मौसम में फल सूखकर उड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। चिल्ली के बीज का स्वाद चार की चिरौंजी जैसा होता था। मैं और वर्षा दीदी मंदिर प्रांगण में जाकर ढेर सारी चिल्लियां बटोर किया करते थे। फिर घर आकर उनमें से बीज निकालकर खाया करते थे। मां समझाती थीं कि "ज्यादा बीज मत खा लेना नहीं तो पेट दुखेगा।" लेकिन बचपन में ऐसी हिदायतओं की भला किसे परवाह रहती है? वैसे भी बचपन में पाचन शक्ति भी तगड़ी होती है। खेलना, कूदना और सब कुछ पचा लेना, यही तो विशेषता होती है बचपन की। मैं तो यूं भी बचपन से ही खिलंदड़ी किस्म की थी। अवसर पाते ही घर से बाहर कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलने जा पहुंचती और तब तक खेलती रहती जब तक मां डांट कर, वापस घर चलने को नहीं कहतीं। यद्यपि मां की आज्ञा की अवहेलना मैंने कभी नहीं की इसलिए पहली डांट पर ही सीधे घर का रास्ता पकड़ लेती।
आज उन बचपन के दिनों से समयनं बहुत दूर आ चुका है। लेकिन हनुमान जी और मदार साहब के बीच के सौहार्द्र की छाप आज भी मेरे मानस में मौजूद है। शांति, अपनत्व और हरियाली का संदेश देती चिल्लियां आज भी मेरे मन के आंगन में उड़ती रहती हैं।
----------------------------
#DrMissSharadSingh #columnist #डॉसुश्रीशरदसिंह #स्तम्भकार #शून्यकाल #कॉलम #shoonyakaal #column #नयादौर